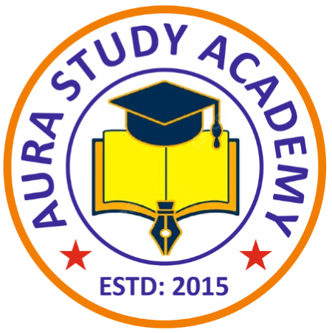प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में मॉरीशस की दो दिवसीय यात्रा के दौरान भारत और मॉरीशस ने अपनी साझेदारी को “वर्धित रणनीतिक साझेदारी” के रूप में उन्नत करने का निर्णय लिया। इसे हिंद महासागर क्षेत्र में द्वीपीय देशों के साथ भारत के गठबंधन को मजबूत करने की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है, जहां चीन अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है।
चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण की योजना भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि भारत एक निचले प्रवाह क्षेत्र (लोअर रिपेरियन स्टेट) में स्थित है। यह स्थिति केवल भारत और चीन के बीच ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान सहित अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी जल-साझाकरण समझौतों की समीक्षा करने और जल कूटनीति की जटिलताओं का विश्लेषण करने की आवश्यकता को उजागर करती है।
ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी अंतरराष्ट्रीय नदियाँ क्षेत्रीय स्थिरता के महत्वपूर्ण कारक हैं, और प्रभावी जल कूटनीति साझा संसाधनों पर सहयोग को बढ़ावा देने और संघर्ष को कम करने में सहायक हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय नदियों के जल उपयोग पर 1966 के हेलसिंकी नियम इन नदियों के उपयोग के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आइए, भारत के पड़ोसी देशों के साथ प्रमुख जल-साझाकरण संधियों का विश्लेषण करें।
सिंधु जल संधि
हाल ही में सिंधु जल संधि (IWT) चर्चा में रही है क्योंकि पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में भारत की दो जलविद्युत परियोजनाओं – किशनगंगा और राटले परियोजनाओं – के डिज़ाइन को लेकर आपत्ति जताई थी।
सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। इसे विश्व बैंक की मध्यस्थता में करवाया गया था और इसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में हस्ताक्षरित किया था। इस संधि ने सिंधु नदी प्रणाली के न्यायसंगत प्रबंधन की रूपरेखा तैयार की, जिससे दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के बावजूद जल संसाधनों के वितरण को सुनिश्चित किया गया।
संधि के अनुसार, भारत को पूर्वी नदियों – रावी, ब्यास और सतलुज – पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों – सिंधु, झेलम और चेनाब – का अनन्य अधिकार प्राप्त हुआ। हालांकि, भारत को जलविद्युत उत्पादन जैसे “गैर-उपभोक्ता उपयोगों” के लिए इन नदियों का सीमित उपयोग करने की अनुमति दी गई।
इस संधि का महत्वपूर्ण हिस्सा “स्थायी सिंधु आयोग” (Permanent Indus Commission) है, जिसके माध्यम से दोनों देश जल संबंधित डेटा का आदान-प्रदान करते हैं और छोटे विवादों का समाधान करते हैं। विवाद समाधान की तीन-चरणीय प्रक्रिया भी स्थापित की गई है – पहला चरण स्थायी आयोग है, दूसरा विश्व बैंक द्वारा नियुक्त “तटस्थ विशेषज्ञ” (Neutral Expert) और अंतिम उपाय के रूप में स्थायी पंचाट न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) है।
2023 में, भारत ने पहली बार पाकिस्तान को इस संधि में “संशोधन” के लिए नोटिस जारी किया। यह कदम इस्लामाबाद द्वारा संधि के कार्यान्वयन में लगातार आपत्तियाँ उठाने के कारण उठाया गया था। 2016 में उरी हमलों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि “रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते”, जिससे भारत की जल कूटनीति में एक रणनीतिक बदलाव का संकेत मिला।
भारत-बांग्लादेश जल साझाकरण समझौते
भारत और बांग्लादेश 54 नदियों को साझा करते हैं। इन नदियों के प्रबंधन के लिए 1972 में इंडो-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग (JRC) की स्थापना की गई थी।
मानसून के दौरान, दोनों देशों के जल संसाधन मंत्रालय बाढ़ पूर्वानुमान और नदी जल वितरण पर मिलकर कार्य करते हैं। 12 दिसंबर 1996 को भारत और बांग्लादेश ने गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें नदी के जल के निष्पक्ष वितरण की गारंटी दी गई थी। हालांकि, हाल ही में गंगा जल प्रवाह में कमी और भारत द्वारा बनाए गए बांधों को लेकर बांग्लादेश असंतोष व्यक्त करता रहा है।
तीस्ता नदी जल समझौता एक और महत्वपूर्ण संधि है, लेकिन 2011 से यह वार्ता ठप पड़ी है क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं। तीस्ता नदी पर बांग्लादेश काफी हद तक निर्भर है, जबकि पश्चिम बंगाल का तर्क है कि अगर तीस्ता का जल बांग्लादेश को दिया गया तो उत्तर बंगाल में लाखों लोग प्रभावित होंगे।
भारत-नेपाल जल साझाकरण व्यवस्था
भारत और नेपाल के बीच जल सहयोग 1894 में ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुआ था। इसके तहत सरदा समझौते के अंतर्गत बनबसा बैराज का निर्माण किया गया था।
1954 में कोसी समझौते के तहत नेपाल में हनुमाननगर बाढ़ नियंत्रण बैराज बनाया गया था, लेकिन नेपाल ने 1966 में संप्रभुता और सिंचाई जल प्राप्ति को लेकर संशोधन की मांग की। इसी तरह, गंडक समझौते (1959) में भी 1964 में संशोधन किया गया था।
1996 में महाकाली संधि ने कई समझौतों को मिलाकर पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना की नींव रखी, लेकिन राजनीतिक कारणों से नेपाल के लिए जल अधिकार सुनिश्चित करने में अब भी कठिनाइयाँ बनी हुई हैं।
भारत-भूटान जलविद्युत सहयोग
भारत और भूटान के बीच जलविद्युत सहयोग को मजबूत बनाने की नींव 1961 में जलढाका परियोजना के साथ रखी गई थी। 1987 में, चुखा जलविद्युत परियोजना (336 MW) पूरी तरह से भारत द्वारा वित्तपोषित (60% अनुदान और 40% ऋण) के तहत विकसित की गई थी।
इसके बाद, ताला जलविद्युत परियोजना (1,020 MW) को भी इसी मॉडल पर विकसित किया गया। 2006 में भारत-भूटान जलविद्युत सहयोग समझौता हस्ताक्षरित किया गया, जिसमें भारत और भूटान ने 2020 तक जलविद्युत उत्पादन क्षमता को 5,000 MW से 10,000 MW तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा।
भूटान की अर्थव्यवस्था में जलविद्युत का महत्वपूर्ण योगदान है, जो देश के कुल निर्यात का 63% हिस्सा बनाता है और यह भारत की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सहायक है।
भारत की जल कूटनीति की रणनीति
भारत की जल कूटनीति ने अब तक क्षेत्रीय सहयोग और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाए रखा है।
भारत ने सिंधु जल संधि, गंगा जल संधि और महाकाली संधि जैसी संधियों के माध्यम से जल साझाकरण की रूपरेखा तैयार की है, लेकिन एक ऊपरी प्रवाह राज्य (Upstream State) होने के बावजूद यह हमेशा स्पष्ट लाभ की स्थिति में नहीं रहा है।
इसके विपरीत, चीन जल साझाकरण पर अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करने से कतराता रहा है। इसका उदाहरण मेकोंग नदी पर उसकी नीति में देखा जा सकता है।
इन चुनौतियों को देखते हुए, भारत को जल साझाकरण पर चीन के साथ निष्पक्ष वार्ताओं को मजबूत करने और पड़ोसी देशों के साथ मौजूदा समझौतों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे।
Source: Indian Express