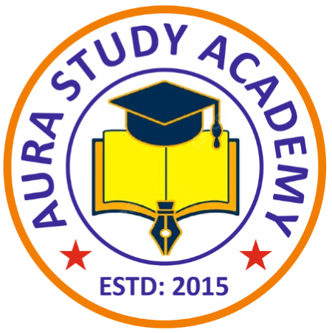भारत की जनगणना अब 2027 में की जाएगी। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। 2021 में होने वाली जनगणना COVID-19 महामारी के कारण स्थगित हुई थी।
इस बार पहली बार स्वतंत्र भारत में जातिगत जनगणना भी की जाएगी, जिसकी मांग विपक्षी दलों ने की थी।
विशेषज्ञों के अनुसार, महामारी के बाद देश सामान्य स्थिति में आ गया था, इसलिए 2023 से ही जनगणना शुरू की जा सकती थी। 2027 तक की देरी को वे अकारण मानते हैं।
जनगणना में देरी से शासन और विकास योजनाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। अब भी नीतियां 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित हैं जबकि जनसंख्या, प्रवास, शहरीकरण और प्रजनन दर में काफी बदलाव आ चुका है।
स्कूल नामांकन अनुमान, टीकाकरण लक्ष्य, और सामाजिक कल्याण योजनाएं जैसे PDS और MGNREGS पुराने आंकड़ों के कारण प्रभावी नहीं हो पा रही हैं।
भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होने जा रही है, जिससे डेटा जल्दी और सटीक रूप से जुटाया जा सकेगा। लेकिन इसके साथ डिजिटल पहुंच न होने के कारण ग्रामीण और वंचित वर्गों के छूट जाने का खतरा भी है।
डिजिटल प्रक्रिया को सहयोगी के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से घर-घर जाकर जानकारी जुटाना अब भी जरूरी है, खासकर ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में।
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) और नागरिक रजिस्टर (NRC) को जनगणना के साथ जोड़ना प्रक्रिया को जटिल बना सकता है और इसे अलग करना बेहतर होगा।
जातिगत आंकड़े जुटाना आसान हो सकता है यदि प्रशिक्षित गणनाकार हों, जो उपनाम और जाति में फर्क समझते हों और उत्तरदाता से सही जानकारी निकाल सकें।
2011 की सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना में लगभग 40 लाख अलग-अलग जातियों के नाम सामने आए थे। इस बार यदि अच्छी तरह योजना बनाकर और प्रशिक्षण देकर गणना की जाए, तो जातिगत डेटा विश्वसनीय हो सकता है।
जनगणना समाज में हो रहे तेजी से बदलाव, जैसे शहरीकरण, प्रवास, जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या की वृद्धावस्था को समझने और संसाधनों के न्यायसंगत आवंटन के लिए जरूरी है।
जनगणना को हर 10 वर्षों में कराना पर्याप्त है, लेकिन इसे समय पर और नियमित रूप से कराना जरूरी है क्योंकि नीति-निर्माण इसी पर आधारित होता है।
Source: The Hindu